26 नवम्बर 1949 - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के संविधान पर अपने विचार
सबसे पहला प्रश्न यह है और इस पर वाद-विवाद हो चुका है कि यह संविधान किस श्रेणी का है। मैं स्वयं उस श्रेणी को कोई महत्व नहीं देता हूं जो इस संविधान को दी जायेगी कृचाहे आप उसे फेडरल संविधान कहें या एकात्मक शासन तंत्र का संविधान कहें या और कुछ कहें। जब तक संविधान हमारे प्रयोजनों की पूर्ति करता है तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिये यह कोई बन्धन नहीं है कि हम एक ऐसा संविधान रखें जो संसार के संविधानों की ज्ञात श्रेणियों के पूर्णतया अनुरूप हो। हमें अपने देश के इतिहास के कुछ तथ्यों को लेना पड़ेगा और इतिहास के तथ्यों जैसी इन वास्तविकताओं का इस संविधान पर कोई कम प्रभाव नहीं पड़ा है।
हम एक गणराज्य बना रहे हैं। भारत में प्राचीन काल में गणराज्य थे, पर यह व्यवस्था 2000 वर्ष पूर्व थी इससे भी अधिक समय पूर्व थी और वे गणराज्य बहुत छोटे-छोटे थे। जिस गणराज्य की हम अब स्थापना कर रहे हैं उस गणराज्य जैसा गणराज्य हमारे यहां कभी नहीं था, यद्यपि उन दिनों में भी और मुगल काल में भी ऐसे साम्रान्य थे जो देश के विशाल भागों पर छाये हुये थे। इस गणराज्य का राष्ट्रपति एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। हमारे यहां ऐसे बड़े राज्य का निर्वाचित मुखिया कभी नहीं हुआ जिसके अन्तर्गत भारत का इतना बड़ा क्षेत्रा आ जाता है। और यह प्रथम बार ही हुआ है कि देश के तुच्छ से तुच्छ और निम्न से निम्न नागरिक को भी यह अधिकार मिल गया है कि वह इस महान राज्य के राष्ट्रपति या मुखिया के योग्य हो और बने जो आज संसार के विशालतम राज्यों में गिना जाता है।
हमने वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की है जिसके द्वारा प्रान्तों में विधान-सभाओं और केन्द्र में लोक सभा का निर्वाचन होगा। कुछ लोगों ने इस बात के प्रति संदेह किया है कि वयस्क मताधिकार बुद्धिमानी की बात होगी। यद्यपि मैं इसे एक ऐसे प्रयोग के रूप में देख रहा हूं जिसके परिणाम के सम्बन्ध में आज कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता है पर मैं इससे आश्चर्य चकित नहीं हुआ हूं। मैं एक ग्रामीण व्यक्ति हूं और यद्यपि अपने कार्य के कारण मुझे बहुत अधिक समय तक नगरों में रहना पड़ा है परन्तु मेरी जड़ अब भी वहीं है। अतः मैं उन ग्रामीण व्यक्तियों से परिचित हूं जो इस महान निर्वाचक-मंडल का एक बड़ा भाग होगा। मेरी सम्मति में हमारे इन लोगों में बुद्धि और साधारण ज्ञान है। उनकी एक संस्वृफति भी है जिसको आज की आधुनिकता में रंगे हुए लोग चाहे न समझें पर है वह एक ठोस संस्कृति। वे साक्षर नहीं हैं और पढ़ने लिखने का मंत्रावत् कौशल उनमें नहीं है। पर इस बात में मुझे रंचमात्रा भी सन्देह नहीं है कि यदि उनको वस्तुस्थिति समझा दी जाये तो वे अपने हित तथा देश के हित के लिये उपक्रम कर सकते हैं। कुछ बातों में तो मैं वास्तव में उनको किसी भी कारखाने के श्रमिक से भी अधिक चतुर समझता हूं जो अपने व्यक्तित्व को खो देता है और जिस यंत्रा का उसे संचालन करना पड़ता है न्यूनाधिक रूप से वह उसी यंत्र का एक भाग बन जाता है। अतः मेरे मन में इस बात के प्रति कोई सन्देह नहीं है कि यदि उनको वस्तुस्थिति समझा दी जाये तो वे केवल निर्वाचन की बारीकियों को ही नहीं समझेंगे बल्कि बुद्धिमानी पूर्वक अपना मत भी देंगे और इसलिये इनके कारण भविष्य के प्रति मुझे कोई शंका नहीं है। अन्य उन लोगों के प्रति मैं यह बात नहीं कह सकता हूं जो नारों द्वारा तथा उनके सामने अव्यावहारिक कार्यक्रमों के सुन्दर चित्रा रखकर उन पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करें। पिफर भी मेरा यह विचार है कि उनका पुष्ट साधारण ज्ञान वस्तुस्थिति को ठीक-ठीक समझने में उनकी सहायता करेगा। अतः हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे विधान-मंडलों में ऐसे सदस्य होंगे जो वास्तविकता से परिचित होंगे और जो वस्तुस्थिति पर यथार्थ दृष्टिकोण से विचार करेंगे।
संविधान में हमने एक न्यायपालिका की व्यवस्था की है जो स्वाधीन होगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त करने के लिये इससे अधिक कुछ और सुझाव देना कठिन है। अवर न्यायपालिका को भी किसी बाह्य प्रभाव से मुक्त रखने का संविधान में प्रयास किया गया है। हमारा एक अनुच्छेद राज्य की सरकरों के लिये कार्यपालिका के कृत्यों को न्यायिक कृत्यों से पृथक करने के विषय को प्रस्तुत करने के कार्य को सरल कर देता है और उस दण्डाधिकारी न्यायालय को, जो आपराधिक मामलों पर विचार करता है, व्यवहार-न्यायालयों के आधार पर लाने के कार्य को सरल कर देता है।
कुछ विशेष विषयों को निपटाने के लिये हमारे संविधान में कुछ स्वाधीन अभिकरणों की योजना की गई है। अतः इसमें दोनों संघ और राज्यों के लिये लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई है और इन आयोगों को स्वतंत्रा आधार पर रखा है जिससे कि कार्यपालिका से प्रभावित हुए बिना ये अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।
एक और स्वाधीन प्राधिकारी नियंत्राण-महालेखा परीक्षक है जो हमारी वित्त व्यवस्था की देखभाल करेगा और इस बात पर ध्यान रखेगा कि भारत या किसी भी राज्य के आगमों के किसी अंश का बिना समुचित प्राधिकार के किसी प्रयोजनों या मदों के लिये उपयोग न हो और जिसका यह कर्तव्य होगा कि वह हमारे हिसाब-किताब को ठीक रखे।
इस संविधान की दो अनुसूचियों में अर्थात् 5 और 6 अनुसूचियों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्राण के लिये विशेष उपबन्ध रखे गये हैं। आसाम को छोड़कर अन्य राज्यों में की जनजातियों के और जनजाति-क्षेत्रों के विषय में जनजाति मंत्राणादात्री परिषद् के द्वारा जन-जातियां प्रशासन पर प्रभाव डाल सकेंगी। आसाम की जनजातियों के और जनजाति क्षेत्रों के विषय में जिला परिषदों और स्वायत्त शासी प्रादेशिक परिषदों के द्वारा उनको अधिक व्यापक शक्तियां दे दी गई हैं। राज्य मंत्रालयों में एक मंत्री के लिये भी आगे और उपबन्ध है जिस पर जन-जातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण का भार होगा और एक आयोग उस रीति के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके अनुसार इन क्षेत्रों पर प्रशासन किया जाता है। इस उपबन्ध का बनाना इस कारण आवश्यक था कि जनजातियां पिछड़ी हुई हैं और उनको रक्षा की आवश्यकता है और इस कारण भी कि अपनी समस्याओं को सुलझाने की उनकी अपनी ही रीति है और जन-जातिवत् जीवन बिताने का उसका अपना ढंग है। इन उपबन्धों ने उनको पर्याप्त संतोष प्रदान किया है।
संघ और राज्यों के प्रशासी तथा अन्य कार्यों के सब रूपों में संघ और राज्यों में परस्पर शक्ति तथा प्रकार्यों के विभाजन संबंधी विषय को इस सविधान में बड़े विवरण पूर्ण ढंग से लिया गया है।
उन समस्याओं में से एक समस्या जिनके सुलझाने में संविधान सभा ने बहुत समय लिया देश के राजकीय प्रयोजनों के लिये भाषा सम्बन्धी समस्या है। यह एक स्वभाविक इच्छा है कि हमारी अपनी भाषा होनी चाहिये और देश में बहुत सी भाषाओं के प्रचलित होने के कारण कठिनाइयों के होते हुए भी हम हिन्दी को अपनी राज भाषा के रूप में स्वीकार कर सके हैं जो एक ऐसी भाषा है जिसे देश में सबसे अधिक लोग समझते हैं। जब हम यह विचार करते हैं कि स्विट्जरलैंड जैसे एक छोटे से देश में तीन राजभाषाओं से कम राज भाषा नहीं हैं और दक्षिणी अप्रफीका में दो राजभाषाएं हैं तो मैं इस विनिश्चय को एक बड़े ही महत्वपूर्ण विनिश्चय के रूप में देखता हूं। देश को एक राष्ट्र के रूप में संघटित करने के दृढ़ निश्चय की ओर सुविधा-क्षमता की भावना इस बात से प्रकट होती है कि वे लोग जिन की भाषा हिन्दी नहीं है उन्होंने स्वेच्छापूर्वक इसे राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया है। अब भाषा के आरोपण करने का प्रश्न ही नहीं है। अंग्रेशी राज्य में अंग्रेशी और मुस्लिम राज्य में पफारसी कचहरी और राज की भाषायें थीं। यद्यपि लोगों ने इन भाषाओं का अध्ययन किया और उनमें विशेष योग्यता प्राप्त की, पर कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि उनको इस देश के अधिकांश लोगों ने स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किया। अपने इतिहास में पहली बार इस समय हमने एक भाषा स्वीकार की है जिसका समस्त राजकीय प्रयोजनों के लिये सारे देश में प्रयोग होगा और मुझे यह आशा करने दीजिये कि यह उन्नत होकर एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा का रूप धारण करे जिसमें सबको समान रूप से गौरव मिले, और इसके साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्रा को अपनी निजी भाषा की उन्नति करने की स्वतन्त्राता ही नहीं होगी वरन् उसको उस भाषा को उन्नत बनाने के लिये प्रोत्साहित भी किया जायेगा जिसमें उसकी संस्वृफति और परम्परा पवित्रा रूप से स्थापित है। व्यावहारिक कारणों वश इस अन्तर्कालीन समय में अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य समझा गया और इस विनिश्चय से किसी को निराश नहीं होना चाहिये जिसको व्यावहारिक विचारों के आधार पर किया गया है। अब यह इस समूचे देश का कर्तव्य है और विशेष कर उनका जिनकी भाषा हिन्दी है कि इसको ऐसा रूप दें और इस प्रकार से विकसित करें कि यह एक ऐसी भाषा बन जाये जिसमें भारत की सामाजिक संस्वृफति की पर्याप्त तथा सुन्दर रूप में अभिव्यक्ति हो सके।
हमारे संविधान की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी अधिक कष्ट के बिना संशोधन किया जा सकता है। यहां तक कि संविधानिक संशोधन भी ऐसे कठिन नहीं हैं जैसे कुछ अन्य देशों में हैं। और इस संविधान में के बहुत से उपबन्धों का संशोधन तो साधारण अधिनियमों द्वारा संसद कर सकती है और संविधानिक संशोधनों के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है। इस समय एक ऐसा उपबन्ध रखा गया था जिसमें यह प्रस्थापित किया गया था कि इस संविधान के प्रवृत्त होने के बाद पांच वर्ष तक इसमें संशोधन करना सरल बना दिया जाये पर इस कारण ऐसा उपबन्ध अनावश्यक हो गया कि इस संविधान में संविधानिक संशोधनों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के बिना संशोधन करने के लिये अनेक अपवाद रख दिये गये हैं। समष्टि रूप से हम एक ऐसा संविधान बना सके हैं जो मेरा विश्वास है कि देश के लिये उपयुक्त सिद्ध होगा।
हमारे निदेशक सिद्धान्तों में एक विशिष्ट उपबन्ध है जिसको मैं बहुत महत्व देता हूं। हमने केवल अपने लोगों की भलाई के लिये ही उपबन्ध नहीं बनाये हैं वरन् अपने निदेशक तत्वों में हमने यह निर्धारित किया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का, अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। संघर्षों से जर्जरित संसार में, एक ऐसे संसार में जो दो विश्व यद्धों के संहार के पश्चात् अब भी शान्ति और सद्भावना स्थापित करने के लिये शस्त्राकरण में विश्वास कर रहा है, यदि हम राष्ट्रपिता की शिक्षाओं का सच्चे रूप में पालन करें और अपने संविधान के इस निदेशक तत्व पर चलें कि यह निश्चित है कि हम अवश्य ही एक महान् कार्य करने में सपफल होंगे। इन कठिनाइयों के होते हुए भी जो हमें घेरे हुये हैं और एक ऐसे वातावरण के होते हुए भी जो हमारा मार्ग भली प्रकार रोक सकता है हे ईश्वर! तू हमें इस मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि और शक्ति दे। हम स्वयं अपने में और उस स्वामी की शिक्षाओं में विश्वास रखें जिसका चित्रा मेरे सर पर टंगा हुआ है और केवल अपने देश की ही नहीं वरन् इस सारे संसार की आशाओं को हम पूरा करेंगे और केवल अपने देश के ही नहीं वरन् सारे संसार के सर्वोत्तम हितों के प्रति हम सच्चे सिद्ध होंगे।
ऐसी केवल दो खेद की बातें हैं जिनमें मुझे माननीय सदस्यों का साथ देना चाहिये। विधान मंडल के सदस्यों के लिये कुछ अर्हतायें निर्धारित करना मैं पसंद करता। यह बात असंगत हैं कि उन लोगों के लिये हम उच्च अर्हताओं का आग्रह करें जो प्रशासन करते हैं या विधि के प्रशासन में सहायता देते हैं और उनके लिये हम कोई अर्हता न रखें जो विधि का निर्माण करते हैं सिवा इसके कि उनका निर्वाचन हो। एक विधि बनाने वाले के लिये बौ(क उपकरण अपेक्षित हैं और इससे भी अधिक वस्तुस्थिति पर संतुलित विचार करने की स्वतंत्राता-पूर्वक कार्य करने की सामर्थ्य की आवश्यकता है और सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि जीवन के उन आधारभूत तत्वों के प्रति सच्चाई होकृएक शब्द में यह कहना चाहिये कि चरित्राबल हो ;वाह, वाहद्ध। यह संभव नहीं है कि व्यक्ति के नैतिक गुणों को मापने के लिये कोई मापदण्ड तैयार किया जा सके और जब तक यह संभव नहीं होगा तब तक हमारा संविधान दोषपूर्ण रहेगा। दूसरा खेद इस बात पर है कि हम किसी भारतीय भाषा में स्वतंत्रा भारत का अपना प्रथम संविधान नहीं बना सके। दोनों मामलों में कठिनाइयां व्यावहारिक थीं और अविजेय सिद्ध हुई। पर इस विचार से खेद में कोई कमी नहीं हो जाती है।


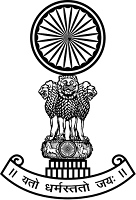

Comments
Post a Comment