राष्ट्रगीत "वन्देमातरम " के बिना अधूरे हैं मूल कर्तव्य और अधिनियम 1971
राष्ट्रगीत ‘‘वन्देमातरम्" के बिना अधूरे है मूल कर्त्तव्य और अधिनियम 1971
संविधान सभा भारत में लागू ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, यहां तक कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को भी रद्द अथवा परिवर्तित कर सकती थी।( पृष्ठ 29 : हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि - सुभाष काश्यप (2015) संविधान सभा की पहली बैठक 09 दिसम्बर, 1946 को हुई थी। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए।
भारत के संविधान निर्माण के इतिहास में 24 जनवरी 1950 एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन संविधान सभा द्वारा तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। भारत के राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत की घोषणा व भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया - जिस गान के शब्द तथा स्वर ‘जन-गण-मन’ के नाम से विख्यात है वह भारत का राष्ट्रगान है किन्तु उस के शब्दों में सरकार की आशा से यथोचित अवसर पर हेर-फेर किया जा सकता है। वंदेमातरम् के गान का जिसका भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम में ऐतिहासिक महत्व रहा है, ‘जन-गण-मन’ के समान ही सम्मान किया जाएगा और उस का पद उसके समान ही होगा (हर्षध्वनि)। मुझे आशा है कि इस से सदस्यों को संतोष हो जायेगा (संविधान सभा 24.1.1950)।
राष्ट्रगीत ‘वन्देमातरम्’ के ऐतिहासिक महत्व का संक्षिप्त परिचय देना यहां युक्तियुक्त होगा। 1882 में बंकिम चन्द चटर्जी ने ‘‘आनन्द मठ’’ उपन्यास में वन्देमातरम् लिखा। यह बंगाली व संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी सरकार ने वन्देमातरम् गीत पर ही नहीं वन्देमातरम् नारे के उच्चारण पर भी प्रतिबंध लगाए। कोई भी वन्देमातरम् का नारा लगाते पाया जाता तो उससे पांच रुपये जुर्माना किया जाता था, जुर्माना न देने वालों को बेतों से पीटा जाता था। 1906 में बारीसाल में निकाले गये जुलूस में वन्देमातरम् का नारा लगाने वालों को पुलिस ने पीट-पीट कर लहुलुहान कर दिया था। श्री अरविन्द ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1909 में किया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में राजनैतिक मंच से गाया गया। 1905 में वन्देमातरम गाने पर प्रतिबन्ध के बावजूद गाया गया। 1907 में बंगाल से श्री अरविन्द ने ‘‘बन्देमातरम्’’ नामक पत्रिका निकाली, जिसमें निष्क्रिय प्रतिरोध पर श्री अरविन्द ने लेख लिखें, जिसके सिद्धांत को बाद में महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध अपनाया था। लाहौर से लाला राजपतराय ने भी ‘वन्देमातरम्’ नामक पत्रिका निकाली थी। 1907 में भीकाजी कामा ने जर्मनी में पहला तिरंगा फहराया जिसके मध्य में वन्देमातरम् लिखा था। इस सभा में पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर भी शामिल थे। नेताजी सुभाषचन्द बोस ने वन्देमातरम् को आजाद हिन्द फौज का गीत बनाया जिसका प्रसारण सिंगापुर रेडियो स्टेशन से कराया गया था। 1976 में भारत सरकार ने एक टिकट जारी किया जिसमें वन्देमातरम् गीत की कुछ पंक्तियां लिखी गयी थी। 1992 से सांसद सदस्य रामनाइक के प्रयासों से संसद का अन्तिम सत्र वन्देमातरम् की धुन से सम्पन्न होना शुरू हुआ। मध्यप्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2005 से सभी मंत्रालयों व कलैक्ट्रेट कार्यालयों में वंदेमातरम् गायन के आदेश पारित किए।
वंदेमातरम् पर संविधान सभा के वक्तव्य और इसके ऐतिहासिक महत्व के अनुसार भारत के संविधान के मूल कर्त्तव्यों में राष्ट्रगीत को सम्मिलित नहीं करना संविधान सभा का अपमान है। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि बिना राष्ट्रगीत के मूल कर्त्तव्य न केवल अधूरे है बल्कि असंवैधानिक है। भारत के संविधान में मूल कर्त्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्त्तव्यों की प्रेरणा रूस के संविधान से ली गई थी। रूस एक साम्यवादी देश है। रूस के संविधान के अनुच्छेद 62 में धरती माता की रक्षा करना प्रत्येक रूसी नागरिक का कर्त्तव्य बताया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल कर्त्तव्यों का संशोधित स्वरूप होगा। अनुच्छेद 51(क) मूल कर्त्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह - (क) ‘‘संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का आदर करें’’।
इसी प्रकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में राष्ट्रगीत के गायन को रोकने पर सजा का उल्लेख नहीं होने से राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान स्थान व सम्मान देने से वंचित रखा है। अधिनियम 1971 को इस उद्देश्य से बनाया गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के गौरव को सर्वोपरी रखें व इनके अपमान होने की स्थिति में दोषी को दण्डित करें। अधिनियम 1971 की धारा 3 राष्ट्रीय गान के गायन को रोकने में यह प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभी में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
अधिनियम 1971 की धारा 3 व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण के पठन पर ज्ञात होता है कि धारा 3 संज्ञेय व अजमानतीय अपराध बनता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्र गान के अपमान करने वाले के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है। परन्तु राष्ट्रगीत के गायन को रोकने की स्थिति में भारत गणराज्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।
अधिनियम 1971 की धारा 3 व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण के पठन पर ज्ञात होता है कि धारा 3 संज्ञेय व अजमानतीय अपराध बनता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्र गान के अपमान करने वाले के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है। परन्तु राष्ट्रगीत के गायन को रोकने की स्थिति में भारत गणराज्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।
जन-गण-मन और वन्देमातरम् को समान स्थान व समान सम्मान दिया जाना भारत गणराज्य से अपेक्षित है। भारत की संसद से यह अपेक्षा है कि 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दिए गए व्यक्तव्य का सम्मान करते हुए राष्ट्रगीत को मूल कर्त्तव्यों व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में जोड़ें। इसके साथ ही भारत सरकार के गृहमंत्रालय की वेबसाइट पर राष्ट्रगीत ‘वन्देमातरम्’ के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी अपलोड करावें।


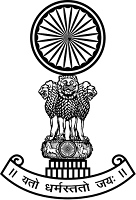

Comments
Post a Comment