संविधान और न्यायालयों में भारतीय दर्शन-1
माननीय सर्वोच्च न्यायालय] नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय में सवेरे सामूहिक प्रार्थना असतो मा सदगमय ॥ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ मृत्योर्मामृतम् गमय ॥ को हिन्दू कहकर यह मांग की गई है कि सेकुलर भारत के विद्यालयों में प्रार्थना नहीं की जा सकती। भारत देश में गणतंत्र राज्य में इस प्रकार की याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न केवल सुना बल्कि बृहद पीठ को सुनने के लिए सिफारिश भी की है। यह कार्यवाही कई प्रश्न खड़े करती है। प्रथम याचिकाकर्ता सामूहिक प्रार्थना के अर्थ को बिना समझे केवल इसलिए की यह संस्कृत में है] इसलिए सेकुलर भारत के विद्यालयों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता] के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। दूसरा माननीय न्यायालय ने भी इस प्रार्थना को सही अर्थ में न समझते हुए याचिकाकर्ता जैसी ही मानसिकता दिखाते हुए बृहद पीठ को भेजने की सिफारिश की है। सर्वोच्च न्यायालय के नीति वाक्य यतो धर्मस्ततो जयः एवं भारत के नीति वाक्य सत्यमेव जयते पर भी याचिका दायर हो तो आज की सर्वोच्च न्यायालय की मानसिकता एवं रूझान को देखते हुए आश्चर्य नहीं होगा कि इन नीति वाक्यों को भी बृहद पीठ को भेजने की सिफारिश कर दी जावें। क्योंकि दोनों ही संस्कृत भाषा में है।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका भारत की शिक्षा प्रणाली एवं विधि शिक्षा के परिक्षण के लिए अवसर प्रदान करती है। संविधान सभा के वाद-विवाद को विधि शिक्षा में जोड़ने की आवश्यकता को जाहिर करती है। संविधान सभा के वाद-विवाद के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए भारत की एकता और अखण्डता को सर्वोपरि रखा गया। सामाजिक क्रांति के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बहस का स्वागत किया। भारत के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपरोक्त दोनों नीति वाक्यों पर कम से कम वर्ष में एक बार निबन्ध लेखन प्रतियोगिता की जरूरत बताती है] जिसके लिए पं- मदन मोहन मालवीय, जिन्हें भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया] के जन्मदिवस 25 दिसम्बर पर सत्यमेव जयते पर निबन्ध प्रतियोगिता रखी जा सकती है] क्योंकि मालवीय जी के प्रयासों से ही सत्यमेव जयते आमजन के मानस तक पहुंचा था] जिसे गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से भारत का नीति वाक्य घोषित किया गया। 6 मई को भारत रत्न से सम्मानित डॉ- पाण्डूरंग वमन काणे के जन्मदिवस पर यतो धर्मस्ततो जयः विषय पर खुली बहस रखी जा सकती है। धर्मशास्त्र का इतिहास जैसी महान कलाकृति की रचना डॉ- काणे द्वारा की गई है। इसी प्रकार संविधान में भारतीय सभ्यता के चित्रण को भी संविधान दिवस 26 नवम्बर को हर क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। संविधान में भारतीय सभ्यता के चित्रण से स्पष्ट है कि संविधान सभा भावी पीढ़ी से अपेक्षा करी होगी कि गणतंत्र भारत भारतीय इतिहास को वैदिक काल से सभ्यता के रूप में समझे।
कुछ सुझाव और भी है जिनके द्वारा न्यायालयों में भारतीय दर्शन के माध्यम से भारतीय मानसिकता से जोड़ा जा सकता है। मीमांसा सिद्धांत द्वारा व्याख्यान को विधि शिक्षा के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, जिससे कि भारतीय बौद्धिकता के प्रति हीन भावना को दूर किया जा सके। साथ ही साथ धर्मशास्त्र के इतिहास को भारतीय न्यायिक इतिहास का अभिन्न अंग बनाकर पढ़ाया जाए। न्यायालयों की भाषा भी सहज एवं सरल हो जिसके लिए मातृभाषा या राजभाषा हिन्दी में न्यायालयों की कार्रवाई सम्पादित की जा सकें। इसके प्रयास किए जाने चाहिए, जैसाकि संविधान सभा के वाद-विवाद को पढ़ने से मालूम होता है।
संविधान
सभा के वाद-विवाद को पढ़ने
पर इसे पांच
भागों में बांटकर
समझा जा सकता
है।
भारत
के संविधान को
संविधान सभा के वाद-विवाद के माध्यम
से समझे
|
|||||
हम
भारत के लोग
- वर्तमान पीढ़ी द्वारा लिए
जाने वाले निर्णय
|
|||||
क्रसं.
|
संविधान सभा द्वारा निर्णय
लिया जा चुका
है।
|
विषय जिन पर संसद
को निर्णय लेना
है।
|
विषय जिन पर वैकल्पिक
समाधान की आवश्यकता
है।
|
विषय जिनका क्रियान्वयन अपेक्षितनहीं हुआ ।
|
विषय जिन पर न्याय
पालिका को निर्णय
लेना है।
|
1
|
अस्पष्टता का निषेध
|
अनुच्छेद 370 और 35ए
|
आरक्षण(आर्थिक आधार , आदि )
|
हिन्दी राजभाषा
|
वेद और गीता
का विद्यालयों में
पढ़ाया जाना।
|
2
|
महिलाओं को समान
अधिकार
|
राष्ट्रगीत वंदेमातरम् की औपचारिक
घोषणा
|
विद्यालयों और महाविद्यालयों
में एनसीसी की
अनिवार्यता
|
उच्च न्यायालय में मातृभाषा/
राजभाषा में निर्णय
|
आस्था, परम्परा और धर्म
पर लक्ष्मण रेखा
|
3
|
वयस्क मताधिकार
|
समान सिविल कोड
|
विधायिका के लिए
न्यूनतम अर्हताऐं
|
शिक्षा का अधिकार
|
भारतीय एकता और अखण्डता
एवं विचारों की
स्वतंत्रता
|
संस्कृत भाषा को भारत की राजभाषा बनाने के लिये पं. लक्ष्मीकांत मैत्र ने कहा : ‘‘अध्यक्ष महोदय, मैं इस उद्देश्य से यह संशेधन उपस्थित कर रहा हूं कि संस्कृत के अध्ययन से हमारे प्राचीन वैभव का पुरावर्त्तन हो। हमें अपना संदेश पश्चिम को भी सुनाना चाहिये। पश्चिम भौतिकवाद की सभ्यता को अपनाये हुये है। हमें पश्चिम को गीता का, वेदों का, उपनिषदों तथा तंत्रों का और चरक तथा सश्रुत आदि का संदेश सुनाना चाहिये। इन्हीं बातों के कारण संसार हमारा आदर करने लगेगा, न कि राजनैतिक वाद-विवादों अथवा वैज्ञानिक खोजों के कारण जो उनकी खोजों की तुलना में कुछ भी नहीं है। रताध्वस्त पश्चिमी देशों में नैतिकता तथा धार्मिक अथवा आध्यात्मिक जीवन भी विनिष्ट हो गया है। और व पथ प्रदर्शन के लिये आपकी ओर देख रहे हैं। स्थिति यह है और इस स्थिति में संसार आपसे संदेश चाहता है। आप अपने दूतावासों द्वारा विदेशों को क्या संदेश देने जा रहे हैं। वे नहीं जानते हैं कि आपके राष्ट्रीय कवि कौन हैं, आपकी भाषा क्या है और आपके पूर्वजों ने किन विषयों में आद्वितीय उन्नति
की थी।’’
की थी।’’
बिन्दु संख्या 2 :- मीमांसा सिद्धांतों द्वारा व्याख्या
इस
विषय पर भारत
के सर्वोच्च न्यायालय
के पूर्व न्यायाधीश
श्री मार्कण्डय काटजू
का मानना है
कि मीमांसा सिद्धांतों
द्वारा व्याख्या भारतीय दर्शन
का अभिन्न अंग
है, जिसमें मैक्सवेल
के सिद्धांतों की
कमी को पूरा
किया जा सकता
है। मीमांसा के
सिद्धांत 2500 वर्ष पुराने
है जिसमें एकीकरण,
समावेश और संसलेशन
इनका आधार है।
इस माध्यम से
न्यायालयों में भारतीय
षड़दर्शन से जुड़ाव
होगा। षड़दर्शन के
छह मुख्य विभाग
है - न्याय दर्शन,
वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन,
योग दर्शन, वेदान्त दर्शन और
मीमांसा दर्शन। भारतीय न्यायिक
प्रक्रिया में मीमांसा
को शामिल नहीं
करने के दो
कारण मिलते है।
पहला कारण भारतीय
संस्कृति एवं दर्शन
के प्रति हीन
भावना दूसरा कारण
है पश्चिमीकरण के
कारण मीमांसा को
अछूत की नजरों
से देखना। आः
नो भद्राः कर्तव्यो
यन्तु विश्वतः से
प्रेरित हो। मैक्सवेल
को अपनाते हुए
मीमांसा सिद्धांतों को भी
सही सम्मान और
स्थान मिलना चाहिए।
मीमांसा नियमों द्वारा व्याख्या
पर श्री किशोरी
लाल सरकार की
व्याख्यामाला एक पुस्तक
के रूप में
उपलब्ध है। इसमें
श्री के. एल.
सरकार द्वारा 13 भागों
में मीमांसा नियमों
द्वारा व्याख्यान पर सम्बोधन
दिया गया है।
बिन्दु संख्या 3 :- धर्मशास्त्र का इतिहास (History of Dharmshatra)
डॉ.
पाण्डुरंग वामन काणे
(07 मई, 1880-08 मई 1972), जिन्हें सन्
1963 में भारत रत्न
से सम्मानित किया
गया, द्वारा धर्मशास्त्र
का इतिहास (History of Dharmshatra) की रचना
की। इसमें भारत
के प्राचीनकाल एवं
मध्यकाल में धार्मिक
और सामाजिक विधि
व्यवस्था की विस्तार
से चर्चा मिलती
है। यह पांच
खण्डों में विभाजित
एक बृहद ग्रंथ
है। अंग्रेजी में
प्रकाशन भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च
इंस्ट्यिट, पुणे एवं
हिन्दी में प्रकाशन
उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्था, लखनऊ
द्वारा किया गया।
बिन्दु संख्या 4 :- भारत के मूल संविधान में भारतीय सभ्यता का चित्रण
मूल संविधान में वैदिक काल के गुरूकुल का दृश्य रामायण से श्रीराम व माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास से घर वापस आने का दृश्य, श्री कृष्ण द्वारा अर्जून को कुरूक्षेत्र में दिए गए गीता के उपदेश के दृश्यों को दर्शाया गया। इसी प्रकार गौतम बुद्ध व महावीर के जीवन, सम्राट अशोक व विक्रमादित्य के सभागार के दृश्य मूल संविधान में मिलते है। इसके अलावा अकबर, शिवाजी, गुरूगोबिन्द सिंह, टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई के चित्र भी मूल संविधान में है। स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य को महात्मा गांधी की दाण्डी मार्च से दर्शाया है। इसी प्रकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का चित्र मूल संविधान में राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा भारत माता को आजाद कराते हुए के प्रयास का चित्रण मूल संविधान में मिलता है।
यह
भारत के सर्वोच्च
न्यायालय का नीति
वाक्य है, जिसे
महाभारत से लिया
गया है। इसका
अर्थ है जहां
धर्म है वहां
विजय है। भारतीय
संस्कृति, दर्शन, इतिहास और
शास्त्रों में धर्म
शब्द का अर्थ
और आशय पश्चिम
की सेकुलर अवधारणा
से पूर्णतः भिन्न
है। धर्म शब्द
को लेकर अक्सर
वाद-विवाद बनाया
जाता है। इसका
कारण यह होता
है कि धर्म
शब्द की समझ
एवं इसका सही
अर्थ समझने में
कमी रह गई।
इस कारण भारतीय
संस्कृति एवं शास्त्रों
के भी दूरी
बन जाती है।
सम्राट अशोक के
समय धर्म शब्द
को यूनान में eusebeia शब्द से
समझ कर इसका
अर्थ समझा जो
कि नैतिक आचरण
तक सीमित था।
इस कारण पश्चिम
कभी भी भारत
में प्रयुक्त शब्द
धर्म को सही
अर्थ में कभी
भी नहीं समझ
सका। आधुनिक काल
में यही गलती
जारी रही और
आज धर्म शब्द
के लिए पश्चिम
में religion
शब्द का प्रयोग
किया है जो
कि अपूर्ण है
क्योंकि religion
शब्द पंथ एवं
सम्प्रदाय तक ही
सीमित है। 2500 वर्षों
से चली आ
रही त्रुटि लगातार
जारी है, पहले
eusebeia शब्द के
माध्यम से और
आज religion शब्द के
माध्यम से। दोनों
ही पश्चिमी शब्दों
ने धर्म शब्द
को ढक दिया,
जिससे धर्म शब्द
का सही अर्थ
और आशय न
तो पश्चिम वाले
समझ पाये और
ना ही भारत
की आधुनिक शिक्षा
धर्म का समग्रता
से चिंतन दे
पाई। धर्म शब्द
के दुरूपयोग का
दूसरा उदाहरण है
Secularism का हिन्दी
में धर्मनिरपेक्ष शब्द
का उपयोग। यह
जानते हुए भी
कि संविधान में
Secular के लिए
पंथ निरपेक्ष शब्द
का प्रयोग किया
गया है। चार
पुरूषार्थी में से
एवं पुरूषार्थ धर्म
को बताया है।
भारत को समझने
के लिए तीन
शब्दों का ज्ञान
जरूरी है कर्मन,
ब्रह्म एवं धर्म।
बिन्दु संख्या 6 :- सत्यमेव जयते
भारत
सरकार एवं भारत
के सभी उच्च
न्यायालयों का नीति
वाक्य है। सत्यमेव
जयते का प्रयोग
आम जन तक
पहुंचाने का श्रेय
डॉ. मदन मोहन
मालवीय (25 दिसम्बर 1861-12 नवम्बर 1946) को जाता
है जिन्हें वर्ष
2015 में भारत रत्न
से सम्मानित किया
गया। सत्यमेव जयते
के सही अर्थ
समझने से भारतीय
दर्शन में सत्य
की खोज की
यात्रा के बारे
में जानकारी मिलती
है। इससे यह
भी मालूम पड़ता
है कि भारतीय
ऋषि, मनिषि, संत,
महापुरूष, योगी आदि
सभी ने सत्य
की खोज को
मानव जीवन के
चार पुरूषार्थ में
से एक पुरूषार्थ
माना है। साथ
ही साथ सत्य
के विभिन्न रूप
एवं अभिव्यक्ति को
स्वीकार किया है,
जिसको एकम् सतः
विप्रा बहुधा वदन्ति के
रूप में समझा
जा सकता है।
इसी कारण भारत
में सहिष्णुता और
विविधता भारतीय संस्कृति का
अभिन्न हिस्सा रहा है।
अनेकान्त वाद के
सिद्धांत को सत्य
की यात्रा में
महत्वपूर्ण सेतु माना
है। व्यक्ति की
चेतना की प्रगति
के अनुपात में
सत्य का साक्षात्कार
मिलता है। यह
भारतीय अध्यामिकता का मूल
सिद्धांत है।



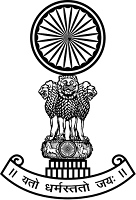

Comments
Post a Comment